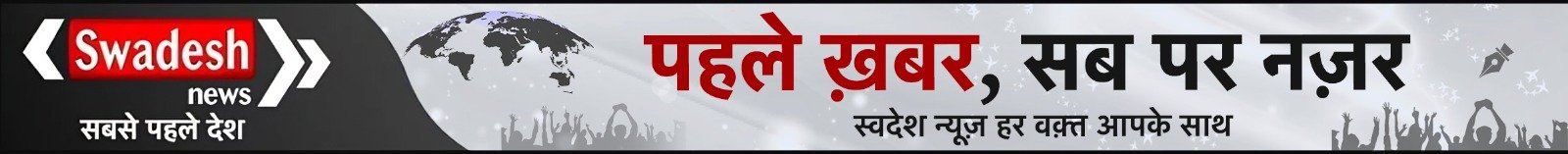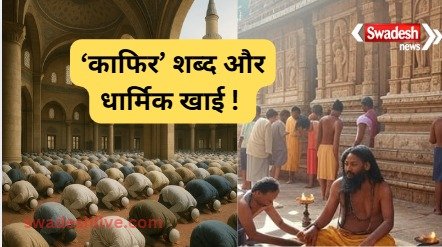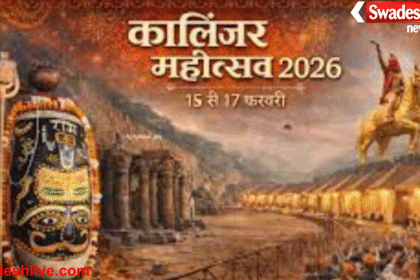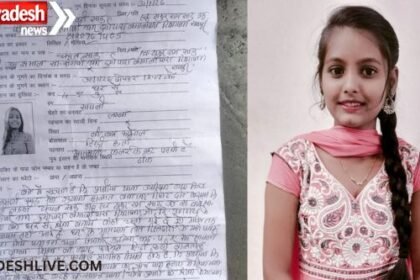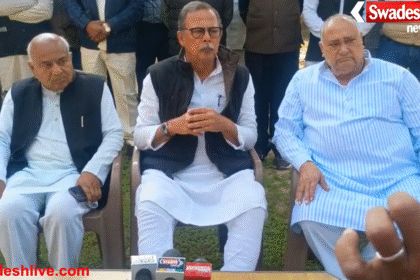“काफ़िर” शब्द का ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव
by: vijay nandan
“काफ़िर” शब्द अरबी भाषा से आया है और मूल रूप से इसका अर्थ होता है “इंकार करने वाला” या “अस्वीकार करने वाला”। कुरान में यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो इस्लाम को नहीं मानते। समय के साथ, इस शब्द का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया गया।
क्या “काफ़िर” शब्द को गलत तरीके से परिभाषित किया गया?
समय के साथ इस शब्द के अर्थ और उपयोग में बदलाव आया है। प्रारंभ में इसका अर्थ केवल ईश्वर के प्रति अविश्वास तक सीमित था, लेकिन बाद में यह शब्द राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में भी इस्तेमाल होने लगा। विशेष रूप से भारत में, मुगलकाल के दौरान और फिर औपनिवेशिक काल में इस शब्द के प्रयोग ने धार्मिक विभाजन को गहराने में भूमिका निभाई।

मुगल शासन और “काफ़िर” शब्द का प्रचार
भारत में मुगलों के शासनकाल के दौरान, “काफ़िर” शब्द का उपयोग मुख्य रूप से गैर-मुसलमानों के लिए किया गया। इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब ने अपने फरमानों और नीतियों में “काफ़िर” शब्द का अधिक प्रयोग किया, विशेष रूप से जज़िया कर लागू करने के संदर्भ में। हालांकि अकबर जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, परंतु औरंगजेब जैसे कट्टर शासकों ने इस शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों के लिए किया, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ा।
धार्मिक खाई और “काफ़िर” शब्द की भूमिका
भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में ऐसे शब्दों का राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग, समाज में नफरत और असहिष्णुता को बढ़ाने का कारण बन सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भी “फूट डालो और राज करो” की नीति के तहत इस धार्मिक ध्रुवीकरण को और गहराया। आज भी, इस शब्द का गलत या उग्रवादी संदर्भों में उपयोग धार्मिक सौहार्द्र के लिए हानिकारक हो सकता है।
“काफ़िर” शब्द और इसकी परिभाषा का विरोधाभास
इस्लामी दृष्टिकोण से “काफ़िर” का अर्थ उन लोगों से जुड़ा है जो इस्लाम और उसके मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि “काफ़िर” को केवल “अल्लाह को न मानने वाला” के रूप में परिभाषित किया जाए, तो इसमें सिर्फ नास्तिक लोग ही आते हैं—जैसे चार्वाक दर्शन को मानने वाले या ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास न रखने वाले।
जबकि हिंदू धर्म तो बहुदेववाद (Polytheism), अद्वैतवाद (Monism), और वेदांत के अनुसार एक निराकार ब्रह्म (Supreme Being) में विश्वास रखने वाला धर्म है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों को “काफ़िर” कहना परिभाषा के स्तर पर एक भ्रम पैदा करता है।
इस्लामी ग्रंथों में “काफ़िर” की व्यापक व्याख्या
कुरान में “काफ़िर” शब्द अलग-अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है—
- जो इस्लाम के संदेश को अस्वीकार करते हैं।
- जो तौहीद (एक ईश्वर में विश्वास) को नहीं मानते।
- जो नबी मुहम्मद के संदेश को नहीं स्वीकारते।
यहाँ एक पेचीदगी उत्पन्न होती है— हिंदू धर्म भी एक ईश्वर (ब्रह्म) को मानता है, लेकिन वह इसे कई रूपों में देखता है। हिंदू धर्म में “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है) जैसी अवधारणाएँ हैं, जो तौहीद से अलग जरूर हैं, लेकिन नास्तिकता नहीं दर्शातीं।
इतिहास और धार्मिक ध्रुवीकरण
मध्यकालीन इस्लामी शासकों ने राजनीतिक और धार्मिक कारणों से इस शब्द का प्रयोग हिंदुओं के लिए किया। हालाँकि, हिंदू दर्शन में स्पष्ट रूप से ईश्वर की उपस्थिति स्वीकार की जाती है, लेकिन चूँकि इस्लामी मान्यताओं के अनुसार मूर्तिपूजा सही नहीं मानी जाती, इसलिए मूर्तिपूजकों को भी “काफ़िर” की श्रेणी में रख दिया गया।
मुगल काल और अन्य इस्लामी साम्राज्यों में यह शब्द हिंदुओं के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ, जबकि हिंदू धर्मग्रंथों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि वे “ईश्वर के विरोधी” हैं। यह पूरी तरह से परिभाषा की व्याख्या और सत्ता के हितों पर निर्भर रहा कि किसे “काफ़िर” कहा जाए और किसे नहीं।

‘काफिर’ नास्तिक शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं के संदर्व में गलत है?
- हिंदू धर्म ईश्वर को मानने वाला धर्म है, इसलिए नास्तिकता की परिभाषा से बाहर है।
- यदि “काफ़िर” का अर्थ अल्लाह को न मानने वाला है, तो यह सिर्फ नास्तिकों के लिए होना चाहिए, न कि किसी भी ईश्वर-विश्वासी के लिए।
- हिंदुओं को “काफ़िर” कहना ऐतिहासिक रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता से जुड़े कारणों का परिणाम रहा है, न कि मूल धार्मिक अर्थ के आधार पर।
- किसी भी शब्द का सही संदर्भ में उपयोग करना आवश्यक है, ताकि गलतफहमियाँ और धार्मिक वैमनस्य न बढ़े।
- हिंदू धर्म के मानने वालों को “काफ़िर” कहना परिभाषागत, धार्मिक और तर्कसंगत रूप से गलत है।
“काफ़िर” शब्द की व्याख्या और उपयोग समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह धार्मिक असहमति को व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुआ, लेकिन बाद में इसका उपयोग राजनीतिक और सांप्रदायिक संदर्भों में किया गया। वर्तमान समय में, इस शब्द के सही संदर्भ को समझना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना ही समाज में शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है।
ये भी पढ़िए; 288 vs 232: संसद ने पास कर दिया वक्फ बिल, अब राज्यसभा में आगे क्या?