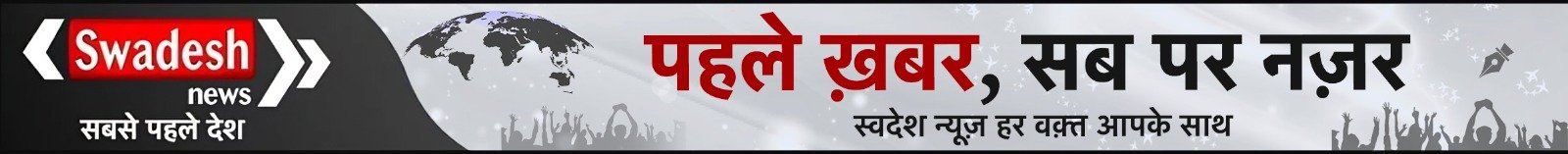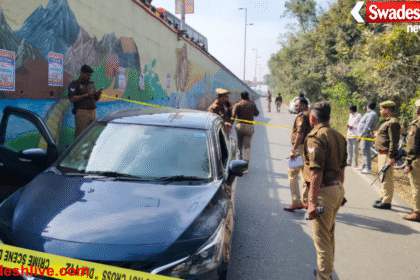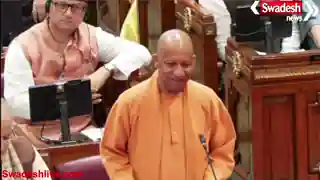नॉर्वे कानून बनाम भारतीय कानून: बच्चे की परवरिश कानून की तुलना हर पहलू से
1. बहस का मुद्दा जरूरी क्यों ?
बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं, और उनकी परवरिश के लिए बनाए गए कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त वातावरण में बड़े हों। नॉर्वे और भारत, दो अलग-अलग सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देश, बच्चों की परवरिश को लेकर अपने-अपने दृष्टिकोण रखते हैं। जहां नॉर्वे एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बच्चों के अधिकारों पर वैश्विक मानकों को अपनाता है, वहीं भारत में कानून पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इस तुलना का उद्देश्य दोनों देशों के कानूनों की विशेषताओं, चुनौतियों और प्रभावों को समझना है ताकि बच्चों के कल्याण के लिए बेहतर नीतियों की दिशा में सोचा जा सके।
2. कानूनी ढांचा और मूल सिद्धांत
नॉर्वे का कानून: नॉर्वे में बच्चों की परवरिश से संबंधित कानून संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों की संधि (UNCRC) पर आधारित हैं। यहां का मूल सिद्धांत “बच्चे का सर्वोत्तम हित” है, जिसे हर नीति और निर्णय का आधार माना जाता है। नॉर्वे का चाइल्ड वेलफेयर एक्ट (Barnevernsloven) बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह कानून राज्य को बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है यदि उनकी भलाई खतरे में हो।
भारत का कानून: भारत में बच्चों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 24 (बाल श्रम पर प्रतिबंध), और अनुच्छेद 39 (बच्चों के कल्याण के लिए निर्देश) से प्रेरित हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों की परवरिश और संरक्षण के लिए मुख्य कानून है। यहां कानून पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आधुनिक चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं।
3. अभिभावक अधिकार और जिम्मेदारियां
नॉर्वे: नॉर्वे में अभिभावकों के अधिकार सीमित हैं और राज्य उनकी परवरिश की शैली पर कड़ी नजर रखता है। उदाहरण के लिए, बच्चों पर शारीरिक दंड देना पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है। बच्चों को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, और अभिभावकों का कर्तव्य उनकी स्वायत्तता और विकास को बढ़ावा देना है।
भारत: भारत में अभिभावकों को पारंपरिक रूप से बच्चों की परवरिश में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि स्कूलों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध है (धारा 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम), घर में इसकी स्थिति अस्पष्ट है और यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। परिवार और समाज का प्रभाव बच्चों की परवरिश में गहराई से जुड़ा हुआ है, और अभिभावक अक्सर बच्चों के भविष्य को अपने निर्णयों से जोड़ते हैं।
4. राज्य की भूमिका और हस्तक्षेप
नॉर्वे: नॉर्वे में चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज (Barnevernet) बच्चों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। यदि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा का संदेह हो, तो राज्य उसे अभिभावकों से अलग कर सकता है और फॉस्टर केयर में रख सकता है। यह नीति विवादास्पद रही है, क्योंकि कई लोग इसे परिवार की स्वायत्तता पर हमला मानते हैं।
भारत: भारत में राज्य का हस्तक्षेप आमतौर पर तब होता है जब बच्चा गंभीर संकट में हो, जैसे अनाथ हो या शोषण का शिकार हो। बाल संरक्षण समितियां और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। हालांकि, जागरूकता की कमी, संसाधनों का अभाव और प्रशासनिक अक्षमता इसे प्रभावी बनाने में बाधा डालते हैं।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार
नॉर्वे: नॉर्वे में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है, और हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त हैं, और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। समानता और समावेशिता इस प्रणाली की पहचान है।
भारत: भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी असमानता दिखती है, जहां गरीब बच्चों को पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती। सामाजिक-आर्थिक कारक इन अधिकारों को लागू करने में बड़ी बाधा हैं।
6. बाल श्रम और शोषण के खिलाफ संरक्षण
नॉर्वे: नॉर्वे में बाल श्रम पर सख्त प्रतिबंध है, और इसका उल्लंघन लगभग न के बराबर है। शोषण के खिलाफ कानून मजबूत हैं, और राज्य इसकी निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र रखता है।
भारत: भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 बाल श्रम को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन गरीबी और अशिक्षा के कारण यह अभी भी एक बड़ी समस्या है। लाखों बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, और कानून का पालन करवाना मुश्किल साबित होता है।

7. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव
नॉर्वे: नॉर्वे की संस्कृति व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। बच्चों को कम उम्र से आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है, और परिवार से ज्यादा व्यक्तिगत विकास पर जोर होता है।
भारत: भारत में परवरिश सामूहिकता और परिवार-केंद्रित होती है। बच्चे परिवार की इज्जत और परंपराओं से जुड़े होते हैं। यहां परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है, जो परवरिश के तरीकों को प्रभावित करता है।
8. कानून लागू करने में चुनौतियां
नॉर्वे: नॉर्वे में राज्य के अति हस्तक्षेप को लेकर आलोचना होती है। खासकर प्रवासी परिवारों के मामले में सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आरोप लगता है, जैसे भारतीय परिवारों के साथ हुए विवाद।
भारत: भारत में कानून का असमान कार्यान्वयन एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और लोगों में जागरूकता का अभाव बच्चों के अधिकारों को लागू करने में रुकावट बनते हैं।
9. तुलनात्मक विश्लेषण
समानताएं: दोनों देश बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अंतर: नॉर्वे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और मजबूत संसाधनों पर निर्भर है, जबकि भारत सामूहिकता और सीमित संसाधनों के बीच काम करता है। नॉर्वे में कानून का पालन सख्त है, वहीं भारत में कार्यान्वयन कमजोर है।
सीखने योग्य पहलू: भारत नॉर्वे से संसाधन आवंटन और सख्ती सीख सकता है, जबकि नॉर्वे भारत से सांस्कृतिक संवेदनशीलता को अपनाने का सबक ले सकता है।
10. निष्कर्ष
नॉर्वे और भारत के बच्चे की परवरिश कानून अपने-अपने संदर्भों में बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। नॉर्वे का ढांचा संसाधन-संपन्न और सख्त है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक लचीलापन कम है। दूसरी ओर, भारत का ढांचा समावेशी और पारंपरिक है, लेकिन संसाधन और कार्यान्वयन में कमी इसे प्रभावी होने से रोकती है। बेहतर भविष्य के लिए भारत को संसाधन बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जबकि नॉर्वे को विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए। अंततः, बच्चों के अधिकारों की सार्वभौमिकता को स्थानीय संदर्भों के साथ जोड़कर ही सही मायनों में उनकी परवरिश सुनिश्चित की जा सकती है।