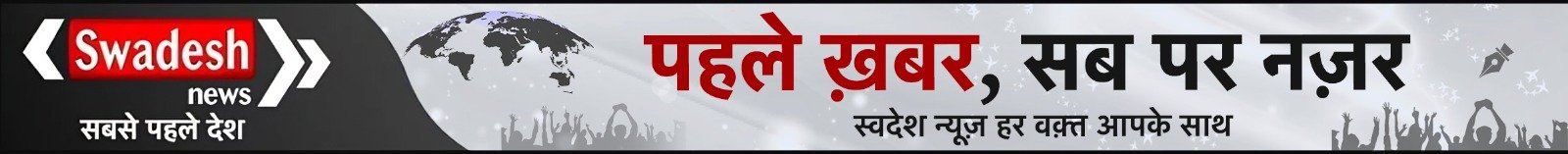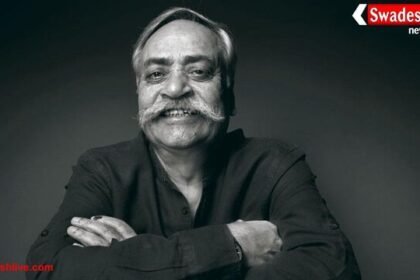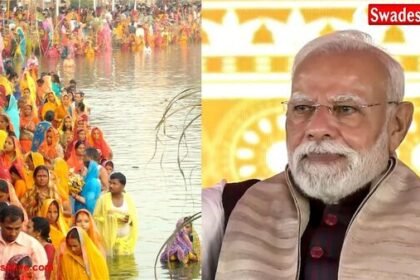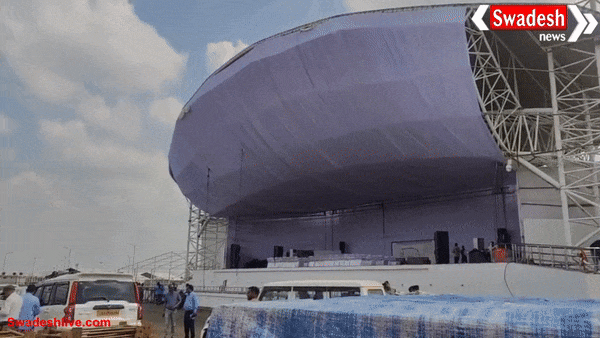आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की, जो इन दिनों भारत के संवैधानिक गलियारों में तूफान मचाए हुए है। जी हाँ, ये है राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट का विवाद! अगर आप सोच रहे हैं कि ये माजरा क्या है, तो चाय की चुस्की लीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही गंभीर भी। तो चलिए, इसे डिटेल में समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे मैं हमेशा आपके लिए लाता हूँ!
पहले समझिए: राष्ट्रपति का रोल क्या है?
सबसे पहले, ये जानना ज़रूरी है कि भारत में राष्ट्रपति का पद क्या होता है। हमारे संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन, क्या वो कोई किंग या क्वीन की तरह सत्ता चलाते हैं? बिल्कुल नहीं! राष्ट्रपति का रोल ज्यादातर औपचारिक होता है। वो वही करते हैं, जो मंत्रिपरिषद (यानी सरकार) की सलाह होती है। फिर भी, कुछ खास मौकों पर उनकी भूमिका सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे:
- प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति: राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं।
- विधेयकों पर हस्ताक्षर: संसद से पास होने वाला कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न करें। वो चाहें तो बिल को वापस भी भेज सकते हैं (अनुच्छेद 111)।
- आपातकाल की घोषणा: चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य में संवैधानिक संकट हो, या वित्तीय आपातकाल, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं।
- क्षमादान की शक्ति: किसी अपराधी की सजा को कम करना या माफ करना भी राष्ट्रपति के अधिकार में है (अनुच्छेद 72)।
लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है! राष्ट्रपति के पास कुछ **विवेकाधीन श0076 शक्तियाँ भी होती हैं, यानी कुछ खास परिस्थितियों में वो अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं। जैसे, अगर संसद में कोई स्पष्ट बहुमत न हो, तो राष्ट्रपति तय कर सकते हैं कि किसे सरकार बनाने का मौका देना है। या फिर, राज्यपाल द्वारा भेजे गए कुछ विधेयकों पर वो अपनी मर्जी से हाँ या ना कह सकते हैं।
अब बात सुप्रीम कोर्ट की
दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है। ये वो जगह है, जहाँ से संविधान की रक्षा होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, और सरकार के हर फैसले की जाँच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ खास शक्तियाँ हैं:
- न्यायिक समीक्षा: अगर संसद या सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है।
- मूल अधिकार क्षेत्र: केंद्र और राज्यों के बीच, या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला करता है।
- अनुच्छेद 142 की ताकत: ये सुप्रीम कोर्ट की वो सुपरपावर है, जिसके तहत वो “पूर्ण न्याय” के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वो सामान्य कानूनों से बाहर क्यों न हो।
सीधे शब्दों में कहें, तो सुप्रीम कोर्ट वो गार्डियन है, जो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का हर नियम पालन हो।
तो विवाद क्या है?
अब आते हैं असली मसले पर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इस केस में तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 विधेयक पास किए थे, लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने इन पर कोई फैसला नहीं लिया और इन्हें राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी इन विधेयकों को लटकाए रखा। तमिलनाडु सरकार ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? ये रहा पूरा ड्रामा:
- तीन महीने की डेडलाइन: कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को तीन महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, तो उन्हें कारण बताना होगा और राज्य को सूचित करना होगा।
- अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुपरपावर (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के उन 10 विधेयकों को सीधे कानून बना दिया, बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के! ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ।
- राज्यपाल को फटकार: कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को जमकर लताड़ा और कहा कि उनका विधेयकों को लटकाना और बार-बार राष्ट्रपति को भेजना “कानूनी रूप से गलत” था।
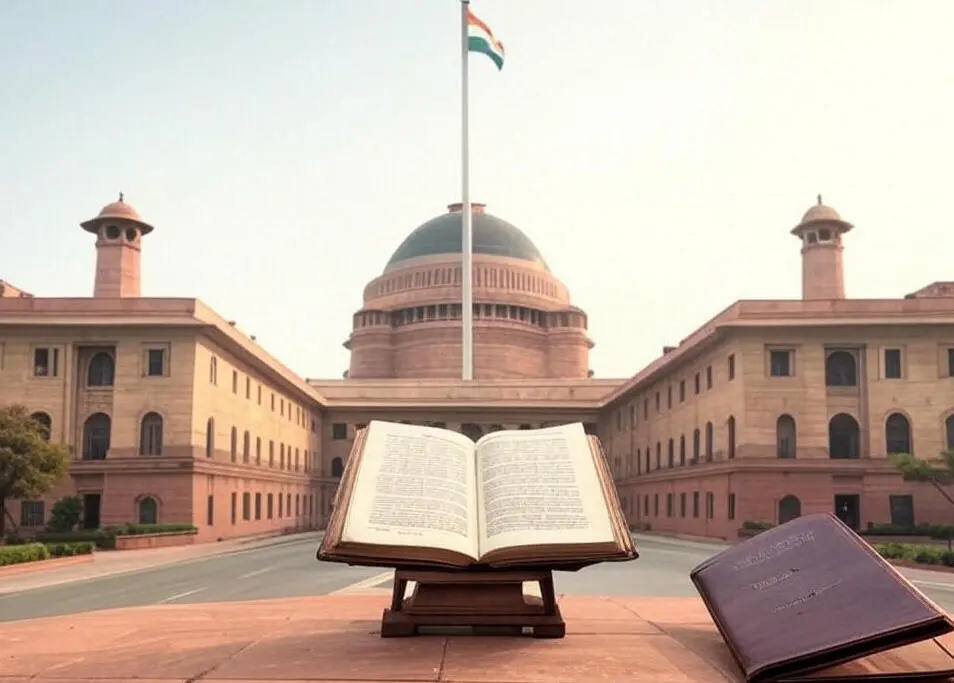
विवाद क्यों बड़ा हुआ?
इस फैसले के बाद देश में दो खेमे बन गए। एक तरफ वो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो, जो इसे न्यायिक अतिक्रमण बता रहे हैं। खास तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। उनके कुछ बड़े बयान ये रहे:
- राष्ट्रपति की शक्ति पर हमला: उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं। उन्हें तीन महीने की डेडलाइन देना उनकी संवैधानिक आजादी को छीनने जैसा है।
- अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग: धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को “लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु बम” कहा। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करके विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दिया।
- सुपर संसद बनने की कोशिश: उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि वो खुद को “सुपर संसद” समझने लगा है, जो संविधान की व्याख्या करने के अपने दायरे से बाहर जा रहा है।
इसके अलावा, पूर्व जज अजय रस्तोगी जैसे कुछ विशेषज्ञों ने भी कहा कि राष्ट्रपति का “पूर्ण वीटो” का अधिकार संविधान में है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस अधिकार को कमजोर करता है। वहीं, दूसरी ओर, कुछ वकील और विशेषज्ञ, जैसे आदिश अग्रवाल, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, लेकिन ये भी कहा कि कोर्ट को पहले राज्यपाल को मौका देना चाहिए था।
इसका असर क्या होगा?
दोस्तों, ये विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं:
- संघवाद पर सवाल: ये फैसला राज्यों के अधिकारों को मजबूत करता है, क्योंकि अब राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी राज्य के विधेयक को अनिश्चितकाल तक लटका नहीं सकते। लेकिन, क्या ये केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ाएगा?
- न्यायपालिका की सीमाएँ: क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या वो सचमुच विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रहा है?
- राष्ट्रपति की भूमिका: क्या राष्ट्रपति का रोल अब सिर्फ रबर स्टैम्प बनकर रह जाएगा, या उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ अब भी मायने रखती हैं?
तो क्या है सही?
अब सवाल ये है कि इस पूरे विवाद में सही कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो कहता है कि वो संविधान और संघवाद की रक्षा कर रहा है? या उपराष्ट्रपति और उनके समर्थक, जो इसे न्यायिक अतिक्रमण बता रहे हैं? मेरी राय में, ये ग्रे एरिया है। एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को ताकत देता है और विधायी प्रक्रिया में देरी को रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ, राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद की गरिमा और स्वायत्तता का भी सम्मान होना चाहिए।
दोस्तों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस पर और स्पष्टीकरण दे सकता है, या फिर संसद कोई नया कानून बना सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है – भारत का लोकतंत्र जितना जटिल है, उतना ही मज़ेदार भी।
Ye Bhi Pade –स्कूल फीस की मार: क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों के लिए?