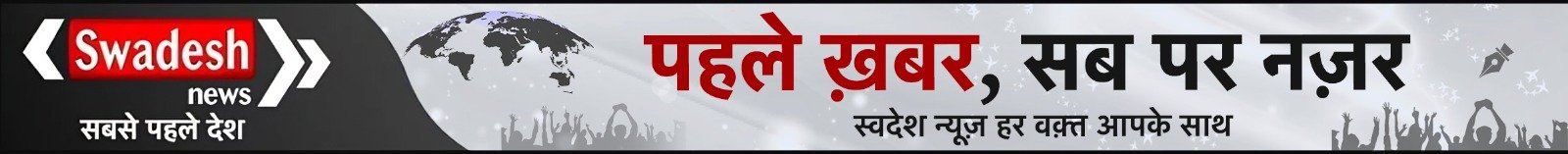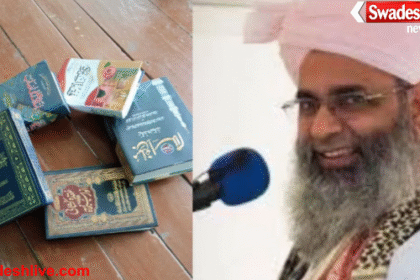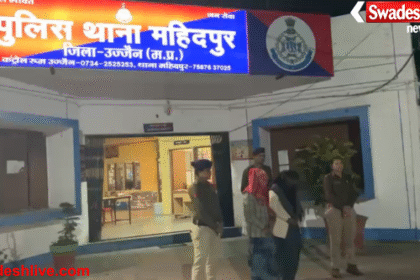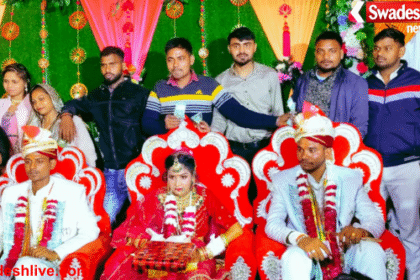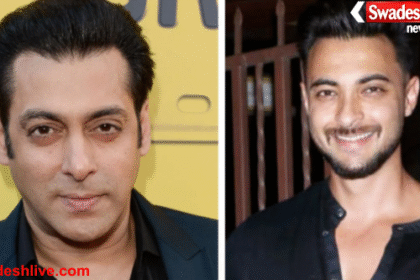चुनावी राजनीति में पॉपुलरिज्म या लोकलुबावनवाद
by: Vijay Nandan
दिल्ली: चुनावी राजनीति में पॉपुलरिज्म (लोकलुभावनवाद) एक ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें नेताओं द्वारा जनता के व्यापक हिस्से की भावनाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को सीधे संबोधित किया जाता है। यह प्रवृत्ति अक्सर “जनता बनाम एलीट” की राजनीति पर आधारित होती है, जहां पॉपुलर नेता खुद को आम जनता के पक्षधर और पारंपरिक संस्थानों, विशेषज्ञों या स्थापित व्यवस्था के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार विधानसभा के चुनावी समीकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, इस चुनाव में रेवड़ी कल्चर की होड़ तो है ही इसके पीछे नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गई है। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा की बजाय पार्टी के सबसे पापुलर चेहरों की लोकप्रियता पर अधिक ध्यान दे रही हैं। बीजेपी जहां विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘लार्जर देन लाइफ’ वाली छवि को आगे कर चुनाव मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि के भरोसे चुनावी अखाड़े में दांव खेल रही है। उधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी राहुल गांधी के चेहरे को सामने कर वोट मांग रही है। राजनीति का ये ट्रेंड भारत में ही चल रहा हो ऐसा नहीं है, दुनिया के लंबरदार अमेरिका में भी चुनावी राजनीति चेहरों की पापुलैरिटी पर आकर फिक्स हो गई है, कमोबेश यही ट्रेंड फ्रांस, इटली, स्वीडन समेत ज्यादातर देशों में देखा गया. भारत में चुनावी राजनीति के बदले ट्रेंड़ पर कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये है कि चेहरों की लोकप्रियता का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि पार्टियों के सिद्धांत कमजोर पड़ गए हैं, विचारधारा हासिए पर ढकेल दी गई है, चुनावों में जनता से जुड़े मद्दे गायब कर दिए गए। भारतीय राजनीति में ये ट्रेंड क्यों पापुलर हुआ, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे।

पॉपुलरिज्म के प्रमुख लक्षण
- जनता का सीधा जुड़ाव: पॉपुलिस्ट नेता आम जनता के मुद्दों को सीधे संबोधित करते हैं, जिससे जनता को ऐसा लगता है कि वे उनके “अपने” नेता हैं।
- एलीट विरोधी रुख: पॉपुलरिज्म का बड़ा पहलू “सत्ता में बैठे लोगों” या तथाकथित एलीट वर्ग का विरोध करना है।
- सरल समाधान: पॉपुलर नेता अक्सर जटिल समस्याओं के आसान और आकर्षक समाधान पेश करते हैं, भले ही वे व्यावहारिक न हों।
- भावनात्मक अपील: यह राजनीति तर्क से अधिक भावनाओं पर आधारित होती है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, और धर्म जैसे मुद्दों को उठाकर जनता की भावनाओं को भुनाया जाता है।
- संदेश का प्रचार: सोशल मीडिया, रैलियां, और जनसंपर्क अभियानों का प्रभावी उपयोग पॉपुलरिज्म की एक बड़ी ताकत है।
पॉपुलरिज्म के फायदे
- जनता की भागीदारी बढ़ाना: यह आम जनता को राजनीति में अधिक रुचि लेने और सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है।
- स्थापित संस्थानों पर चुनौती: पॉपुलरिज्म संस्थानों और परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिससे समाज में बदलाव की संभावना बनती है।
- आम मुद्दों को प्राथमिकता: यह राजनीति अक्सर उन मुद्दों को सामने लाती है जो पारंपरिक राजनीतिक दल अनदेखा कर देते हैं।
पॉपुलरिज्म की चुनौतियां
- लोकलुभावन वादे: कई बार पॉपुलिस्ट नेता ऐसे वादे करते हैं जिन्हें पूरा करना असंभव होता है। इससे जनता का मोहभंग हो सकता है।
- संस्थानों को कमजोर करना: पॉपुलरिज्म के चलते संवैधानिक संस्थानों और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा हो सकता है।
- ध्रुवीकरण: यह राजनीति समाज में विभाजन को बढ़ावा दे सकती है, जैसे जाति, धर्म, या वर्ग के आधार पर।
- अल्पकालिक दृष्टिकोण: पॉपुलर नेता दीर्घकालिक रणनीतियों के बजाय अल्पकालिक और त्वरित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
भारत में पॉपुलरिज्म
भारत में पॉपुलरिज्म का असर हर चुनाव में देखा जा सकता है। विभिन्न दल और नेता जनता को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाएं, आर्थिक सहायता, और सांस्कृतिक-धार्मिक मुद्दों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए:
- मुफ्त योजनाएं: राज्यों में मुफ्त बिजली, पानी, या गैस जैसी योजनाएं पॉपुलरिज्म का हिस्सा होती हैं।
- राष्ट्रीयता और धर्म: चुनावी रैलियों में अक्सर राष्ट्रीयता और धर्म के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।
- लोकलुभावन नारे: “गरीबी हटाओ” से लेकर “सबका साथ, सबका विकास” जैसे नारे जनता के दिल में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
पॉपुलरिज्म चुनावी राजनीति में एक दोधारी तलवार है। एक ओर यह जनता को सशक्त करता है और उन्हें राजनीति का सक्रिय हिस्सा बनाता है, तो दूसरी ओर यह संस्थागत स्थिरता और दीर्घकालिक विकास के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। अतः, लोकतंत्र में पॉपुलरिज्म को समझदारी से अपनाना और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।
ये भी पढिए: दिल्ली चुनाव को लेकर यूपी व हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर