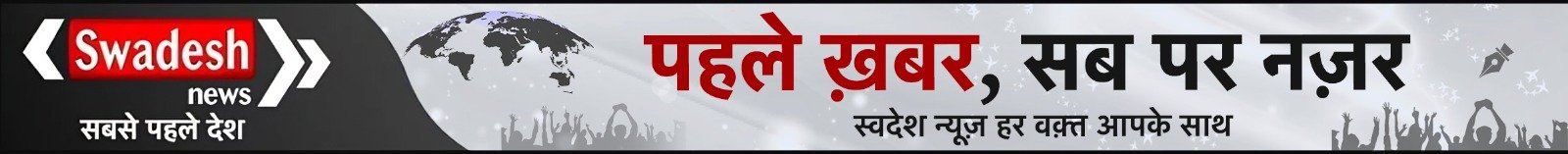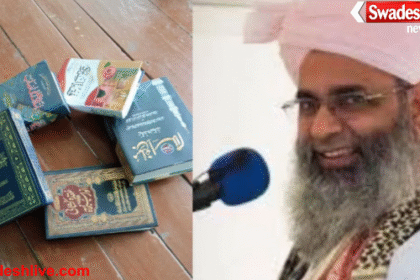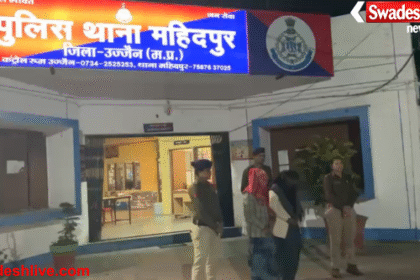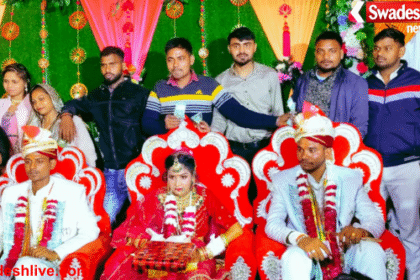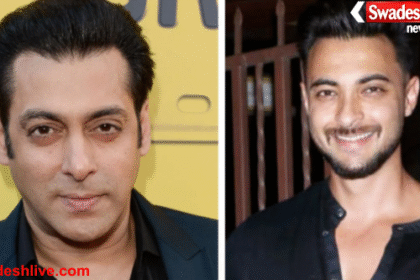भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। फिर भी, संगीत और कला ने बार-बार इन सीमाओं को पार कर लोगों के दिलों को जोड़ा है। इस संदर्भ में, पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियां एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिनमें सूफी परंपरा के साथ-साथ हिंदू भक्ति भावनाओं, विशेष रूप से राधा-कृष्ण के प्रेम का समावेश देखने को मिलता है। उनकी कव्वाली “सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम” इसका जीवंत प्रमाण है। यह लेख भारत में जात-पात से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, नुसरत की कव्वालियों में राधा-कृष्ण के प्रतीकों का उपयोग, और भारत-पाक कलाकारों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है।
जात-पात से ऊपर इंसानियत: भारतीय राजनीति का एक आदर्श
भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्म, जातियां और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। हालांकि, जात-पात और धार्मिक विभाजन ने अक्सर सामाजिक और राजनीतिक एकता को चुनौती दी है। भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरण वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा बन गए हैं, जिससे सामाजिक समरसता कमजोर हुई है। फिर भी, भारतीय संविधान और कई महान नेताओं ने हमेशा समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया है।
सूफी और भक्ति परंपराएं इस दिशा में एक प्रेरणा रही हैं। बुल्ले शाह, कबीर, और मीराबाई जैसे संतों ने अपनी रचनाओं में जात-पात और धार्मिक बंधनों को नकारते हुए प्रेम और एकता का संदेश दिया। नुसरत फतेह अली खान ने इन्हीं संतों की भावनाओं को अपनी कव्वालियों में जीवंत किया, जो न केवल धार्मिक सीमाओं को पार करती थीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक सेतु भी बनाती थीं। उनकी कव्वालियां हमें याद दिलाती हैं कि मानवता और प्रेम किसी भी राजनीतिक या सामाजिक विभाजन से ऊपर हैं।
नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों में राधा-कृष्ण का प्रतीकात्मक उपयोग
नुसरत फतेह अली खान, जिन्हें “शहंशाह-ए-कव्वाली” के नाम से जाना जाता है, ने सूफी संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनकी कव्वालियां सूफी दर्शन के साथ-साथ भारतीय भक्ति परंपरा को भी समेटती थीं। उनकी प्रसिद्ध कव्वाली “सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम” इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कव्वाली में नुसरत ने मीराबाई की भक्ति रचना को अपनाया, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को सूफी भक्ति के साथ जोड़ा गया। गीत के बोल, “शाम बने हैं राधिका, राधा बन गईं शाम,” यह दर्शाते हैं कि प्रेम में प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाता है, जो सूफी दर्शन का मूल है।
यह कव्वाली 1979 में भारत में उनके प्रदर्शन के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। नुसरत ने इस रचना को कव्वाली के रूप में प्रस्तुत कर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बनाया। उनकी कव्वालियों में राधा-कृष्ण के प्रतीकों का उपयोग केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह प्रेम, एकता और आध्यात्मिक समन्वय का प्रतीक था। उनकी एक अन्य कव्वाली, “कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी,” में राधा की कृष्ण के प्रति विरह-भावना को सूफी प्रेम के साथ जोड़ा गया, जो दर्शाता है कि प्रेम की भाषा किसी धर्म या सीमा की मोहताज नहीं होती।
नुसरत की कव्वालियों ने भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। उनकी रचनाएं, जैसे “दम मस्त कलंदर” और “अफरीन-अफरीन,” न केवल सूफी दर्शन को बल्कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों को भी दर्शाती थीं। यह सांस्कृतिक समन्वय आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद कला और संगीत लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।
भारत-पाक कलाकारों की वर्तमान स्थिति
भारत और पाकिस्तान के बीच कलाकारों का आदान-प्रदान हमेशा से सांस्कृतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नुसरत फतेह अली खान ने 1980 के दशक में भारत में कई प्रदर्शन किए और बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। उनकी मृत्यु के बाद, उनके भतीजे राहत फतेह अली खान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राहत ने बॉलीवुड में “तेरे मस्त-मस्त दो नैन,” “जिया धड़क-धड़क,” और “ज़रूरी था” जैसे गीतों के साथ अपनी पहचान बनाई।
हालांकि, हाल के वर्षों में भारत-पाक संबंधों में तनाव के कारण कलाकारों के लिए सीमा पार काम करना मुश्किल हो गया है। 2016 के उरी हमले के बाद, कुछ भारतीय संगठनों ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने में बाधा आई। इसके बावजूद, राहत फतेह अली खान जैसे कलाकारों ने डिजिटल मंचों और अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अपनी कला को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाया।
वहीं, भारतीय कलाकारों को भी पाकिस्तान में प्रदर्शन के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नुसरत ने 1996 में दिल्ली में अपने एक प्रदर्शन के दौरान भारत-पाक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था, “संगीत लोगों को एकजुट करने का अवसर देता है। जितना अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान होगा, उतना ही दोनों देशों के बीच नफरत कम होगी।” उनकी यह बात आज भी प्रासंगिक है।
हाल के समय में, सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे मंचों ने दोनों देशों के कलाकारों को एक-दूसरे के दर्शकों तक पहुंचने में मदद की है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान और भारत ने दोनों देशों के कलाकारों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, राहत फतेह अली खान का गीत “अफरीन-अफरीन” यूट्यूब पर 300 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसमें भारतीय दर्शकों का भी बड़ा योगदान है।
निष्कर्ष
नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम, एकता और मानवता किसी भी सीमा, धर्म या जात-पात से ऊपर हैं। उनकी कव्वालियों में राधा-कृष्ण के प्रतीकों का उपयोग न केवल सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद, संगीत और कला ने हमेशा लोगों को जोड़ा है। आज के समय में, जब जात-पात और धार्मिक विभाजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नुसरत की कव्वालियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत और प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी बंधनों को तोड़ सकती है।
भारत-पाक कलाकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को कम करेगा, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां प्रेम और एकता सर्वोपरि हों। नुसरत फतेह अली खान की विरासत हमें यह सिखाती है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्माओं को जोड़ने का माध्यम है।