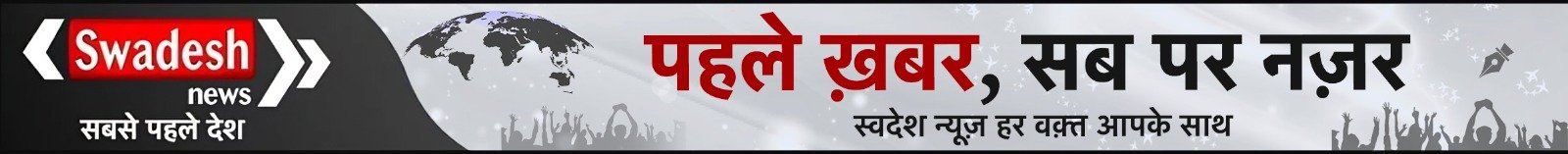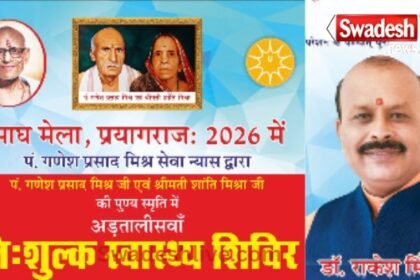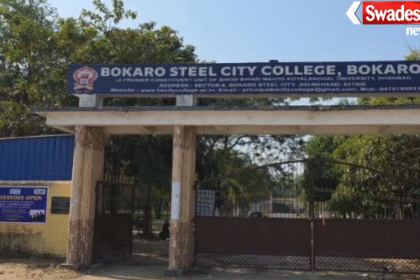झारखंड बना ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की मिसाल
लेखक: हिमांशु प्रियदर्शी, स्टेट एडिटर, स्वदेश न्यूज
झारखंड ग्रामीण महिलाओं के तीव्र सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख रहा है। अक्सर बड़ी आबादी को देश पर बोझ समझा जाता है, परंतु यदि इस मानव संसाधन में निवेश किया जाए तो यही बोझ एक उपयोगी संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। इसके परिणाम बहुआयामी होते हैं। यह न केवल गरीबी का उन्मूलन करता है, बल्कि देश की जीडीपी में भी वृद्धि करता है। यह निवेश तीन मुख्य रूपों में होता है। मानव को शिक्षित करके, उसके भीतर कौशल का विकास कर तथा उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर। एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल नागरिक केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि दीर्घकाल तक निरंतर योगदान देता रहता है।
कोई भी देश पुरुषों और महिलाओं से मिलकर बनता है, लेकिन हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक परंपरा ने महिलाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों में हमेशा पुरुषों की तुलना में पीछे रखा है। स्वास्थ्य की स्थिति तो और भी चिंताजनक रही है। देश की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग पचास प्रतिशत है, लेकिन इस आधी आबादी को हमने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने से लगभग वंचित ही रखा है।
कल्पना कीजिए कि यदि यह आधी आबादी सक्रिय रूप से जीडीपी में योगदान देने लगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा।
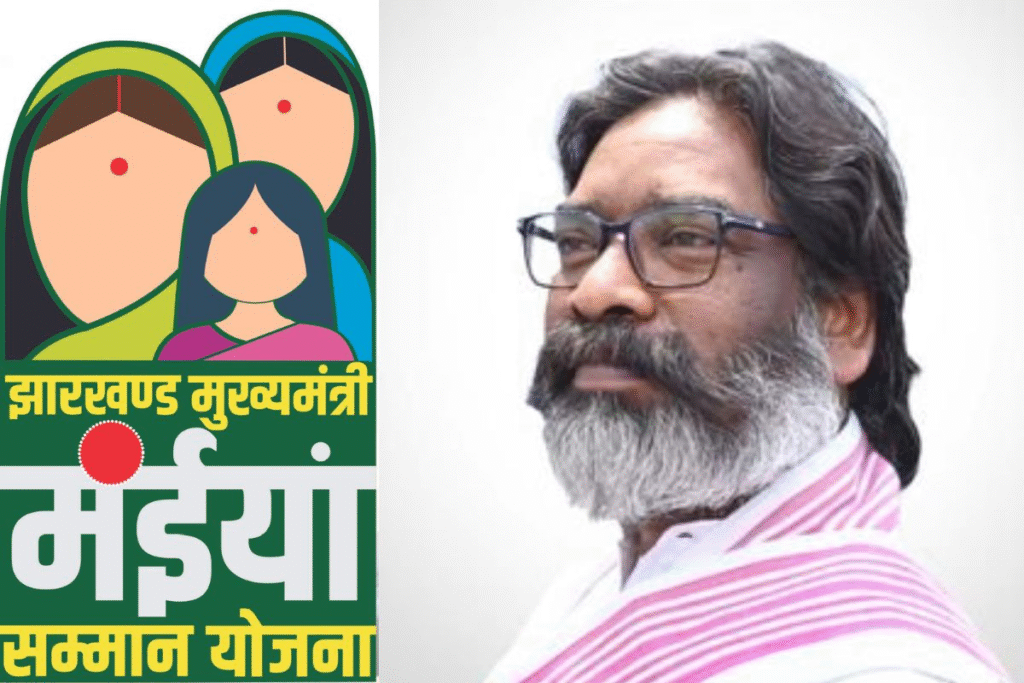
यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारों ने इस अंतर को समझा नहीं, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के बीच की खाई को भरने की जो गति होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखाई दी। नीतियां और कानून तो बने, लेकिन इनका लाभ केवल उन चुनिंदा महिलाओं को मिला जो शिक्षित थीं। वह भी प्रायः शहरी क्षेत्रों की महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं की सुध लंबे समय तक नहीं ली गई।
हालांकि, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस मामले में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रहा है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं विभिन्न प्रकार के रोजगार में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाली झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) अपने नाम के अनुरूप ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सशक्त बना रही है।
यह संस्था महिलाओं को कौशल विकास के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता और ऋण दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। वे महिलाएं, जो पहले या तो दारू-हड़िया बेचती थीं या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी की शिकार थीं—अब आजीविका के ठोस साधनों से जुड़ रही हैं।
इनमें कई महिलाएं जंगल से लाख एकत्रित करती हैं और उनसे सुंदर चूड़ियां, कंगन और आभूषण बनाती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि झारखंड भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, फिर भी इससे बने आभूषणों का व्यवसाय मुख्यतः राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में होता रहा है। अब यह स्थिति बदल रही है।
ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे कम जल और सीमित भूमि में अधिक उपज प्राप्त कर सकें। महिलाएं खेतों में मल्चिंग विधि, माइक्रो ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि का प्रयोग कर रही हैं और विविध फसलों व सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं।
इसके अतिरिक्त वे मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, किराने व वस्त्रों की दुकानों का भी संचालन कर रही हैं।
सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि महिलाएं अब अपने कार्यों की बारीकियों को आत्मविश्वास के साथ साझा करती हैं और बताती हैं कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ी है और जीवन स्तर में कितना सुधार आया है। कुछ शहरों में “दीदी कैफे” के नाम से रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, जिनका संपूर्ण संचालन महिलाएं करती हैं और वहां साफ-सुथरे वातावरण में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है।
इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को खुले बाजार तक पहुंचाने का कार्य भी सरकार स्वयं कर रही है। विभिन्न जिला मुख्यालयों में पलाश केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां इन उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। सरकार के कर्मचारी गांव-गांव जाकर महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करते हैं, वित्तीय सहायता दिलवाते हैं और उनके कार्यों की नियमित निगरानी भी करते हैं।
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि राज्य सरकार प्रशंसा की पात्र है, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है। हालांकि, अभी भी कई कार्य शेष हैं। सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन और विपणन के लिए प्रेरित करे और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, क्योंकि इन शुद्ध उत्पादों की मांग बहुत अधिक है।
महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से अनेक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शिक्षा की महत्ता को पहचानने के बाद महिलाएं अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार होगा, साक्षरता दर बढ़ेगी, स्कूल ड्रॉप-आउट दर घटेगी, कुपोषण की समस्या कम होगी, डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुलभ होगी और इंटरनेट के माध्यम से महिलाएं वैश्विक दुनिया से जुड़ सकेंगी।